वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की आधुनिकता और मेक-इन-इंडिया की मिसाल के रूप में पेश किया गया था। अंदर की एयरक्राफ्ट जैसी सीटें, साफ-सुथरा इंटीरियर और हाई-टेक सुविधाएँ यात्रियों को प्रभावित करती हैं। लेकिन ट्रैक पर चलती ही ट्रेन की असलियत उजागर हो जाती है।
ट्रायल में 180 किमी/घंटा तक की रफ्तार दिखा चुकी वंदे भारत अब कई रूटों पर 60–80 किमी/घंटा की औसत रफ्तार तक सीमित रह जाती है। कुछ मार्गों-जैसे दिल्ली-वाराणसी पर औसत तेज़ (लगभग 95 किमी/घंटा) तो हैं, पर कोयम्बटूर-बेंगलुरु जैसे रूटों पर गति मात्र 58 किमी/घंटा तक सिमट जाती है। यात्रियों का सवाल है: क्या सिर्फ 20–30 मिनट की बचत के लिए महंगा किराया वाजिब है?
मूल कारण पुरानी और ऊबड़-खाबड़ पटरियाँ, मोड़-ढलान, सिग्नलिंग और मालगाड़ियों का साझा उपयोग हैं। देश के बहुसंख्यक ट्रैक 110 किमी/घंटा से अधिक गति के लिए तैयार नहीं हैं। मार्च 2025 तक नेटवर्क में हजारों स्पीड-रिस्ट्रिक्शन पॉइंट दर्ज थे। इस बीच सरकार ने ट्रैक और सुरक्षा में निवेश बढ़ाया है—कई किलोमीटर की पटरियाँ अपग्रेड हुईं, लेवल क्रॉसिंग हटाए गए और कवच जैसी प्रणालियाँ लगाईं गईं—फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि संख्या बढ़ी है पर गुणवत्ता में कमी है।
अब वंदे भारत स्लीपर जैसी महँगी परियोजनाएँ भी सामने हैं, जिनका उद्देश्य 180 किमी/घंटा रफ्तार की रात्री सेवा देना है। पर जब तक बुनियादी ढाँचा और सिग्नलिंग आधुनिक नहीं होंगे, ये ट्रेनें खूबसूरत होटल की तरह ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ती रहेंगी — तेज़ नहीं, मगर महँगी जरूर।
क्या वंदे भारत का असली लाभ तभी मिलेगा जब पटरियाँ, सिग्नल और रख-रखाव की गहराई से तैयारी हो? अपनी राय कमेंट में बताइए।







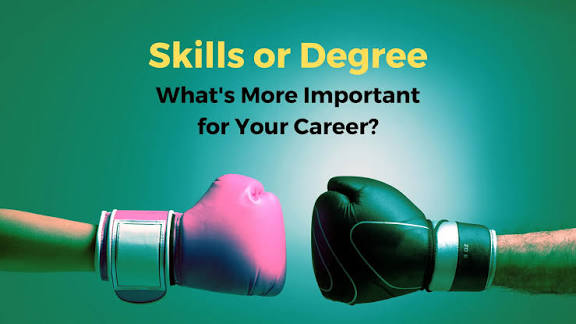







Leave a Reply